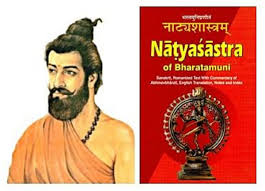
ध्रुवा संगीत: एक अध्ययन
ध्रुवा संगीत: एक अध्ययन

नाट्यशास्त्र रंगमंच को एक अनेक कलाओं के लोकतांत्रिक संगठन के रूप में व्याख्यायित करता है। नाटक मात्र एक कला नहीं अपितु वह कई कलाओं का उत्कृष्ट संयोजन है। मनोहर काले के अनुसार नाट्यशास्त्र हमें जिस कलागत सत्य से अवगत कराना चाहता है वह है उसका ‘संपूर्णता’ का दृष्टिकोण। उसकी धारणा में कला का वास्तविक सौन्दर्य अवयवों में नहीं होता वरन इनके समुचित ‘संयोजन’ में है जो उनमें अंतर्निहित विविधताओं को ‘सामान्यगुण योग’ की कसौटी पर सम्पन्न करता है। यों ‘नाट्य’ शब्द में नृत्य तथा नाटक दो ही शब्दार्थ समाविष्ट है किंतु उभय अर्थो से यह तथ्य दृष्टिगत होता है कि नाटक संगीत , नृत्य, कार्य -व्यापार तथा कविता की एक सर्वतोमुखी कला है।
वी राघवन लिखते हैं कि भरत का नाट्यशास्त्र न केवल प्राचीन भारतीय प्रतिभा की इतनी उत्कृष्ट निष्पत्ति है जितनी कि सांची-शिल्प अथवा अजंता चित्र , अपितु विष्णुधर्मोत्तर के अनुसार परवर्ती कलाओं की नींव भी है। प्राचीन भारत की उच्चतम साहित्यिक रचनाओं , कालिदास एवं शूद्रक की कृतियों , के मूल में यही है। देश के अनेक जीवित प्रादेशिक तथा लौकिक नृत्य नाट्य परंपराओं का रसास्वाद करने के लिए इसकी प्रविधि को हृदयंगम करना आवयश्यक है।
जब आप नाट्यशास्त्र को पढते हैं तब आपको अपनी नाट्य परंपरा पर गर्व भी होता है और वर्तमान दुर्दशा पर क्षोभ भी। क्या नाटक की वत्तर्मान दुर्दशा या कमजोर स्थिति में मजबूती के बीज हमें नाट्यशास्त्र के भीतर से प्राप्त हो सकते हैं? कम से कम कलाओं के उचित समायोजन और संगीत की भूमिका के संदर्भ में तो यह बात स्पष्ट तौर पर कही जा सकती है। भरत ने नाटकों के जिन अवयवों पर विस्तारपूर्वक व्याख्याएं की हैं उनमें संगीत सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में हमारे समक्ष मौजूद है। उन्होंने संगीत पर स्वतंत्र रूप से अध्याय 28 से 33 तक चर्चा की है। किंतु इसके अलावा नाटक में उसके प्रयोग पर पूर्वरंग विधान और ध्रुवा गीतों के रूप में उसकी महत्त्वपूर्ण व्याख्याएं की हैं जिन्हें प्रत्येक साहित्य, रंगमंच और संगीत के विद्यार्थी को अवश्य पढना और समझना चाहिए।
भरत के नाट्यशास्त्र का ध्रुवा वर्णन भारतीय नाट्य-संगीत हेतु एक अन्यतम उपलब्धि है। नाट्यशास्त्र में ध्रुवाओं की चर्चा यों तो कई स्थानों पर है किंतु नाट्यशास्त्र का 32वां अध्याय मुख्यतः इसी पर आधरित है। भरतमुनि के अनुसार ‘नाट्य में गीतों के द्वारा रस संचार को साधने का कार्य नाट्यस्थिति के अनुरोध के साथ रखा जाता हैं तथा इसी से नाट्य में भावदशा की तीव्रता तथा अधिकाधिक अनुभूतिप्रवणता को भी साधा जाता है। गीतों में ध्रुवा का एक विशिष्ट स्थान भरत ने दिखलाया और उनका विस्तार से प्रतिपादन किया। इनमें स्वर तथा वर्णों का उपयुक्त चयन, अलंकारों का समुचित संयोजन, शारीरिक भावभंगिमा और गीत के उत्कर्ष के साथ ध्रुवाओं की रचना रहती है जिससे नाटकीय पात्रों की गति, चेष्टा आदि को पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है। इन कारणों से ध्रुवागान नाट्यप्रयोग के लिये सर्वाधिक उपयोगी हो जाता है। भरत के अनुसार इनमें विनियोजित अंग नाट्यप्रयोग से जुड़ जाते हैं, एक स्थायित्व के साथ और इसी कारण वे ‘ध्रुवा’ कहलाते हैं। ध्रुवा का स्वरूप वर्ण, अलंकार, लय, जाति तथा पाणि की नियमित स्थिति वाला होता है।
वस्तुतः ध्रुवाओं के विस्तृत विवरण से यही प्रतीत होता है कि ये नाट्यप्रयोग में पात्रों के कार्य और मनोभावों को अभिव्यक्ति देने के लिये पाश्र्व संगीत का भी कार्य करतीं थीं। और इनमें रहने वाली अभिव्यंजनाएं गीतों और छंदों में रखी जाती थीं जो कि लोकभाषा में लय और ताल के साथ होती थीं।
प्राचीन काल में विद्यमान नारदादि के सप्तगीत के अंग तुग्, पणिका, गाथा और सप्तगीतांग का जो स्वरूप था वही भरत ने आगे ‘ध्रुवा’ के रूप में विस्तार से दिखलाया है। कवि के द्वारा रचित ‘गीत’ के रूप में रहने से इन्हें उत्तरकालीन आचार्य रामचन्द्र – गुणचन्द्र ने ‘कवि ध्रुवा’ का नाम देकर उनका प्रयोजन नाट्य प्रयोगगत भाव तथा रसादि को समृद्धि देने वाला माना है।
ध्रुवाओं में क्रम विधान सहज है। प्रथम आलाप-तान उसके साथ वाद्य तथा उसके बाद छंदगान, यही क्रम रखा जाता है। ध्रुवा के साथ पुष्कर, मृदंग व उसी जैसे अन्य वाद्यों की संगति की जाती है। गीत के साथ इस वाद्य का वादन किस स्थान से आरम्भ किया जाय इस संबंध में सविस्तार विवरण दिया गया है।
ध्रुवा गान का प्रथम आवर्तन बिना भाण्ड वाद्य की संगत के किया जाता था. ‘सन्निपात’ नामक ताल-स्थान पर मृदंग अथवा पुष्कर का वादन आरम्भ किया जाता था। गीत के साथ मृदंगादि वाद्यों का प्रथम आघात ‘ग्रह’ कहलाता था। इसी ग्रह स्थान को दिग्दर्शित करने के लिए वाद्य पर आघात के साथ अंगुलियों का उपयोग किया जाता था। नाट्य में ध्रुवा गीत विभिन्न स्थलों और स्थितियों में प्रस्तुत किए जाते थे। इस तरह भरत ने धु्रवा के पांच प्रभेद बतलाये हैं-
प्रावेशिकी, नैष्क्रामिकी, आक्षेपिकी, प्रासादिकी, अन्तरा।
प्रावेशिकी- इस ध्रुवा की योजना पात्रों के प्रवेश के समय में होती है। नाट्यार्थ तथा प्रमुख रस से संबंधित गीतवस्तु को यहाँ रखा जाता है।
नैष्क्रामिकी- अंक की समाप्ति पर पात्रों के रंगमंच निष्क्रमण के समय इसे गाया जाता है। यदि पात्र का निष्क्रमण अंक के मध्य में होता हो तो भी नाट्याचार्य अपनी दक्षता के साथ इसका प्रयोग कर सकता है।
आक्षेपिकी- नाट्यप्रयोग में प्रवाहमान रस का अतिक्रमण कर अन्य रस का आक्षेप करने वाली ‘आक्षेपिकी’ ध्रुवा है। इसमें प्रायः द्रुत लय रखी जाती है एवं नृत्य का भी समाविष्ट होता है।
प्रासादिकी – प्रवाहमान रस के अतिक्रमण का परिहार कर यथा स्थिति लाने व दर्शकों का प्रसादन करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसकी योजना प्रेक्षक के चित्त को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। मनः प्रसाद की संपादिका होने के कारण यह ‘प्रासादिकी’ कहलाती है।
आन्तरी- इसका प्रयोग नाट्यप्रयोग के दोषों को दूर करने में होता है। पात्रों के मूच्र्छित हो जाने या वस्त्र-आभूषण आदि धारण करने की क्रिया के बीच जो समय खाली रहे उसमें इस अव्यवस्थित समय क्रम को ढंकने के लिये गीत की योजना रखना ‘अंतरा’ या मध्यवर्ती ध्रुवा कहलाती है।
नाटकों में गीतों को ‘फिलर’ के रूप में आज भी बहुतायत में प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी दृष्य या घटना में जो खाली स्थान रह जाता है उसे भरने के लिए गीत-संगीत का उपयोग कर लिया जाता है। कुछ वैसी ही स्थिति आन्तरी ध्रुवा को लेकर भी है। नाट्यशास्त्रा के महत्त्वपूर्ण व्याख्याकार अभिनवगुप्त ने इसकी व्युत्पत्ति ‘अंतरे च्छिद्रे गीयते इत्यंतरा ध््रुवा’ की है जिसका कार्य छिद्र या दोष का प्रच्छादन भी होता है। परन्तु शारदातनय के मत में इस धु्रवा का नाट्यप्रयोजन्य त्रुटि या दोष का आच्छादन मात्र नहीं अपितु अंक की परिसमाप्ति में इसका गायन भी होता है जो उपसंहारात्मक रूप में हाता है।
नाट्यशास्त्र में ध्रुवाओं के पांच स्थानों की चर्चा है। ये पांच हैं- 1. प्रवेश 2. आक्षेप 3. निष्काम 4. प्रासाद 5. अन्तरा। ये पांचों क्रमशः प्रावेशिकी, आक्षेपिकी, नैष्क्रामिकी, प्रासादिकी, आन्तरी ध्रुवाओं से सम्बद्ध हैं।
पांचो ध्रुवाओं के अंग इस प्रकार रहते हैं- मुख, प्रतिमुख, वैहायसक, स्थित, प्रवृत्त, वज्र, संधि, संहरण, प्रस्तार, उपवर्त, माषघात, चतुरस्र, उपपात, प्रवेणी, शीर्षक, सम्पिष्टक, अन्ताहरण तथा महाजनिक। ये सभी पांच ध्रुवाओं के अंग हैं। इनकी पांच ध्रुवाओं में भरत ने विभाजनपूर्वक योजना भी रखी है। सर्वप्रथम इसमें एक वस्तु जिसमें रहे वह ‘ध्रुवा’, दो वस्तु रहने पर ‘परिगीतिका’, तीन वस्तु के होने पर ‘मंद्रक’ तथा चार वस्तु के रहने पर ‘चतुष्पदा’ समझना चाहिए। ध्रुवाओं के पांचों प्रवेशिकी आदि प्रभेदों में अंगों का विभाजन इस प्रकार है-
प्रावेशिकी ध्रुवा – प्रवृत्त, उपवर्त, वज्र तथा शीर्षक
अंगिता में – प्रस्तार, मापघात, माहाजनिक, प्रवेणी तथा माषघत
अवकृष्टा ध्रुवा में – मुख तथा प्रतिमुख
स्थिता ध्रुवा में – वैहायसक तथा अन्ताहरण।
अन्तरा ध्रुवा में – सन्धि तथा प्रस्तार
उक्त पांच प्रकार की ध्रुवाओं के अलावा भरत ने रस तथा गुणों के आधर पर ध्रुवाओं के अन्य छः प्रभेद किए हैं- 1. शीर्षका 2. उद्धता 3. अनुबंध 4. विलम्बिता 5. अंगिता 6. अपकृष्टा।
ध्रुवाओं में प्रमुख स्थान रखने वाला गीत को ‘शीर्षक’, उद्धत प्रकार से गाये जाने वाले गीत को ‘उद्ध्ता’, किसी नाट्योपचार के लिए प्रयुक्त ध्रुवा को ‘अनुबन्ध’, धीमे वेग के गीत को ‘विलम्बिता’, शृंगार रस को लेकर आरम्भ होने एवं उत्कृष्ट गुणों से युक्त गीत को ‘अंगिता’ एवं किसी अन्य भाव या कारण से भिन्न हो ‘अपकृष्टा’ ध्रुवा कहते हैं।
भरत ने छंदोगत पादों के विस्तार को ध्यान में रखते हुए ध्रुवाओं को रखने की विधि बतलायी जिससे वे उपयुक्त रस, स्थिति तथा विविध शारीरिक चेष्टाओं को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो जाती हैं जैसे देवताओं के निर्विघ्न कार्यों को दिखलाने में अनुष्टप वृत्त का प्रयोग रखते हैं। प्रावेशिकी ध्रुवा में वक्त्रा तथा अपर वक्त्रा वृत्त उपयुक्त होते हैं जबकि पुट और चूलिका जैसे वुत्त नैष्क्रामिकी के उपयुक्त होते हैं। सभी ध्रुवाओं में तीन प्रकार के वृत्त रहते हैं- 1 बहुलगुरू या सर्वगुरू 2. लघु बहुल या सर्व लघु तथा 3. गुरू-लघु मिश्र। अधिकांशतः गुरू वर्णों से निर्मित छन्दों से अपकृष्टा ध्रुवाएं, लघु वर्णों से निर्मित छन्दों में द्रुता ध्रुवाएं और गुरू तथा लघु वर्णों के द्वारा ;मिश्र रूप में निर्मित छंदों में ;इनके अतिरिक्तद्ध शेष ध्रुवाएं होती हैं जो वृत्त अल्प ;लघुद्ध अक्षरों के और अनेक छंदों में होते हैं उनकी योजना स्थितावकृष्टा तथा आक्षेपिकी ध्रुवा में रखी जाती है। इसी प्रकार ओज तथा युग्म प्रमाण वाले छंद आक्षेपिकी ध्रुवा में विनियोजित करते हैं।
भरत ध्रुवाओं के प्रयोग में अनुकूलता को बहुत महत्त्व देते हैं। कब और कौन सी ध्रुवा का किस प्रकार से प्रयोग हो इसके विषय में भरत हमेशा सचेत दिखाई पड़ते हैं। उनके अनुसार किसी नाट्य प्रयोग में रस, भाव,वस्तु,अवस्था, प्रदेश, समय या अवसर तथा पात्रों की मानसिक- अवस्था का उनके विषय, कथावस्तु, प्रयोग तथा पात्रों के अनुसार विचार करने के पश्चात ही इन ध्रुवाओं की योजना करना श्रेयस्कर है।
ध्रुवाओं में रसानुकूलता को लेकर भरत खासे सचेत हैं। विभिन्न ध्रुवाओं का प्रयोग कब हो इस पर भरत ने पर्याप्त विचार किया है। इसको भरत ने दो प्रकारों में विभक्त किया है- एक आत्मस्थ और दूसरा परस्थ। इनमें जब स्वयं को लक्ष्य कर गीत या ध्रुवा गान रहे तो ‘आत्मस्थ’ तथा दूसरे या अन्य को उद्दीस्ट कर ध्रुवा गान हो तो ‘परस्थ’ होगा। इनके आक्षेप से संबद्ध स्थानों को भी बतलाया गया है। मसलन जब केाई पात्र गिर गया हो, बीमार अथवा मूच्र्छित हो गया हो या मर गया हो तब करूण रस की स्थिति में अपकृष्टा ध्रुवा की योजना होनी चाहिए। उसमें भी किसी मृत या घायल पुरूष के प्रत्यक्ष दर्शन से दुख की दशा हो तो ऐसे स्थान पर करूण रस में स्थित या विलम्बित लय में ध्रुवाओं का गान करना चाहिए। वहीं रौद्र, वीर या भयानक आदि रसों को प्रत्यक्ष या सीधे बतलाने में, आवेग तथा संभ्रम भावों की दशा में ध्रुवाओं का द्रुत लय में गान करना चाहिए। किसी को प्रसन्न करने, याचना करने, प्रेमी से प्रथम मिलन के दौरान शृंगार या अद्भुत रस के अवलोकन करने में प्रासादिकी ध्रुवा का मध्यलय में गान रखा जाता है। दुख प्राप्त होने, क्रोध प्राप्त होने या किसी पर शस्त्र संधान करने की दशा में अंतरा ध्रुवा को लगातार या देर तक चालू रखना चाहिए। साथ ही जब गायन या रोदन हो रहा हो या उत्पात सा किसी आश्चर्य की घटना घटित हो तो ऐसे अवसर या स्थान पर पात्रों का प्रवेश बिना ध्रुवा गान के होना चाहिए।
ध्रुवाओं के पात्रानुकूल प्रयोग की बात बताते हुए भरत पात्रों की प्रकृति के तीन विभेद करते हैं- उत्तम, मध्यम तथा अधम। ध्रुवाओं के विषय, स्त्री या पुरुष पात्रों के उत्तम, मध्यम या अधम प्रकारों की स्थिति में उनके अनुरूप उनके गुणों की समानता को ध्यान में रखते हुए रहने चाहिए। विभिन्न रसों की दशा में उत्तम पात्रों की तुलना मत्त गजों तथा राज हंसों से रखी जा सकती है। मध्यम पात्रों की तुलना सारस, मोर, क्रौन्च, चकवा, हंस तथा सरोवर से उनके गुण या स्थिति के अनुसार रखी जाए। अधम पात्रों की उपमा कोकिल, भौंरा, टिटोही ;कुररद्ध, अलूक, बगुला कबूतर और कादम्ब पक्षियों में रखी जाती है।
पात्रों की प्रकृति के अनुकूल ही विभिन्न संकेतों का विवरण भरत ने प्रस्तुत किया है। भरत के अनुसार यह संकेत मुख्यतः सादृश्य गुण पर आधरित रहा करता था। उदाहरण के लिए नृपस्त्री का संकेत शर्वरी, वसुध, ज्योत्स्ना, नलिनी इत्यादि शब्दों से, वेश्यादि का संकेत वल्ली, सारसी, शिखिनी, मुर्गी इत्यादि से तथा अन्य अधम प्रकृति महिलाओं का संकेत भ्रमरी, कोकिला आदि शब्दों से किये जाने के संबन्ध में स्पष्ट विधान नाट्यशास्त्र में है।
संस्कृत नाट्यों की एक विशेषता यह रही है कि उसमें दृश्य विधान न के बराबर रहता है और प्रायः सभी दृश्यों में स्थान व प्रदेशादि की सूचना भी संवादों द्वारा ही दी जाती है। ध्रुवा गीतों का बहुत कुछ उपयोग इन संदर्भों में भी किया जाता था। समय की सूचना देने के लिए कब कौन सी ध्रुवा का गान हो इस संदर्भ में कहा गया है कि पूर्वाह्न को सूचित करने के लिए सौम्य ध्रुवाओं का गान करना चाहिए, मध्याह्न को सूचित करना हो तो दीप्त ध्रुवाओं का गान करना चाहिए और करुण ध्रुवाओं के गान के द्वारा अपराह्न या संध्याकाल को संकेतित या सूचित किया जाता है।
ध्रुवाओं में स्वर, लय और ताल के साथ छंद का विशेष महत्त्व है। बिना छंद के किसी गीत में पदों की योजना नहीं होती अतएव ध्रुवागीत के विषय को देखकर उसको तदनुसार उपयुक्त छंद में रखना चाहिए। सभी तरह की ध्वनि हेतु सांगीतिक वाद्य और स्वर ही साधन थे। अतएव भरत का निर्देश है कि वाहन या यान आदि की गति के प्रदर्शन आदि के संदर्भ में सम्बद्ध ध्रुवा के लिए स्वीकृत या नियोजित छंद के पद के लिये उसी के साथ संगत होने वाला वाद्य वादन रखा जाए जो कि गीत के सभी अंगों की गतियों से तालमेल रखने वाला हो। वास्तव में प्राचीन गीतकों के अंग, कला, तथा छंदों के आधर पर ध्रुवा की उद्भावना होती है। गीतकों के षट्कल तथा अष्टकल विभाग-ध्रुवा में त्रयस्र तथा चतुरस्र ताल का निर्माण करते हैं। ध्रुवा में शब्दों का प्रयोग भावाभिव्यक्ति के लिये आवश्यक माना जाता था। संगीत के आरोहावरोहादि वर्णों का उसी सीमा तक प्रयोग किया जाता था जो अर्थव्यक्ति में बाधक न हों। इसी दृष्टि से केवल कुछ ही गीतालंकार ध्रुवा-गान के लिए उचित माने गए हैं। ध्रुवा का स्थान गांधर्व के निबद्ध संगीत में है, यह बात मननीय है। भरत के अनुसार गांधर्व स्वरतालपदात्मक है तथा उसमे पद स्वर तथा ताल इन दोनों के पोषक हैं।
पद दो प्रकार के माने गए हैं – निबद्ध तथा अनिबद्ध। अक्षरों की नियत संख्या, छन्द तथा यति के नियमों से नियंत्रित पद समूह ‘निबद्ध’ कहलाता है। यति तथा पाद के नियमों से स्वतंत्र तथा आतोद्यों में स्वच्छंद रूप से बजाए जाने वाले अक्षर ‘अनिबद्ध’ कहलाते हैं। वाद्यों पर जिन नानाविध कारणों तथा बोलों का अनिर्बंध रूप से वादन किया जाता है, वही ‘अनिबद्ध’ पद है। आधुनिक वाद्यवादन के पूर्व जो स्वर समुदाय ‘नोम् तोम्’ के रूप में बजाए जाते हैं वे इसी के उदाहरण हैं। इसमें लय अवश्य रहती है, परंतु ताल का बंधन नहीं रहता।
वास्तव में भरतकालीन ध्रुवा गीत ‘शब्द-संगीत’ अथवा ‘काव्य-संगीत’ का श्रेष्ठ निदर्शन है। ध्रुवा गीतों का उद्देश्य अर्थाभिव्यक्ति होने के कारण उसका गान ऐसे प्रसंगों पर किया जाता है जब उसकी उद्देश्य सिद्धि के लिये अनुकूल वातावरण उपस्थित हो। इसीलिए गायन, रूदन, संभ्रम, उत्पात इत्यादि प्रसंगों पर ध्रुवागान अनुपयुक्त माना गया है। भरत के समय के नाटकों में जिस प्रसंग की अभिव्यक्ति कथनोपकथन तथा अन्य तत्सदृश उपादानों से न की जा सकती थी, उसकी अभिव्यंजना ध्रुवा गीतों के माध्यम से की जाती थी। दूसरे शब्दों में गद्य तथा काव्य के द्वारा जिन भावों की अभिव्यंजना असंभाव्य रहती, उनके लिए गीतों का प्रयोग किया जाता था।
ध्रुवाओं की भाषा पर बात करते हुए भरत ने शौरसेनी भाषा के प्रयोग की बात कही है और साथ ही कभी-कभी मागधी भाषा के प्रयोग को भी सहमति दी है। ध्रुवाओं में इन भाषाओं के इस्तेमाल हेतु पात्र की प्रकृति मुख्य कारक थी। यथा दिव्य पात्रों हेतु संस्कृत भाषा एवं मानव पात्रों हेतु शौरसेनी भाषा या अर्धसंस्कृत भाषा को प्रयुक्त किये जाने का प्रावधान था। ध्रुवा हेतु प्राकृत भाषा की उपादेयता नाट्यशास्त्र में स्वीकृत की गई है। केवल देवता विषयक गान अथवा संकीर्तन में संस्कृत भाषा का प्रयोग उपादेय माना गया है। प्रतीत होता है कि नाट्यशास्त्र के पूर्व ही संस्कृत नाटकों के अंतर्गत प्राकृत ध्रुवाओं का प्रयोग उनकी गेयानुकूलता के कारण किया जाता रहा है। कालिदास के नाटकों में उपलब्ध प्राकृत गीत, जिनका गान मालविका, हंसपदिका, परूरवा आदि के द्वारा हुआ है, इसी तथ्य को स्पष्ट करते हैं।
ध्रुवाओं की एक महत्त्वपूर्ण विशेषता उनकी सांकेतिकता में है। जैसा निवेदित किया जा चुका है, ध्रुवाओं का उपयोग उन अर्थों तथा प्रसंगों की अभिव्यक्ति के लिए विहित था, जिनके लिए काव्य निःशक्त सिद्ध होता था। प्रचीन नाट्य के नियमानुसार रंगमंच पर कुछ घटनाओं का प्रदर्शन वर्जित था। तत्कालीन नाट्य की सीमित परिधि के कारण जिन घटनाओं एवं मनोभावों का चित्रण संभव न था, उसी का सम्पूर्ण विवरण गीत की सांकेतिक भाषा में सम्पन्न किया जाता था। आधुनिक रंगमंच पर यही कार्य दृश्य-पट तथा सविस्तार संकेतों के माध्यम से सम्पन्न किया जाता है। इन्हीं अभावों की पूर्ति प्राचीन ध्रुवा गीतों के द्वारा की जाती रही है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि भरत ध्रुवा गीतों का बहुत महीन विवरण करने में सक्षम रहे हैं। नाट्यशास्त्र के प्रमाण के आधार पर कहा जा सकता है कि नाट्यशास्त्र की रचना से पूर्व ध्रुवा गान का प्रचार था तथा नारद जैसे गन्धर्वाचार्यों के द्वारा उसकी विवेचना की जा चुकी है। नारद के नाम से ख्यात ‘नारदी शिक्षा’ में ध्रुवा गीतों के संबन्ध में कथमपि विवेचन नहीं पाया जाता। सम्भवतः गांधर्व की यह परम्परा मौलिक रूप से प्रचलित रही हो और उसी को नाट्यशास्त्र में सर्वप्रथम लेखबद्ध किया गया है। ध्रुवा गीतों की परम्परा का क्रियात्मक रूप भरत के पूर्व से लेकर परवर्ती संस्कृत नाटक-ग्रंथों में बराबर दिखाई पड़ता है। कालिदास के ‘विक्रमोर्वशीयम्’ नाटक में ध्रुवा गीतों का प्राचुर्य है। बाण ने इन गीतों की उज्ज्वल परम्परा का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। यह गान भाव तथा ताल से अनुप्राणित रहता था। दामोदर के कुट्टिनीमत में श्रीहर्ष के रत्नावलि नाटक के प्रत्यक्ष अभिनय का वर्णन किया गया है, जिसमें प्रवेश तथा निर्गमन के समय प्रावेशिकी आदि ध्रुवा गीतों के गाये जाने का उल्लेख है। यानी स्पष्टतौर पर यह कहा जा सकता है कि ध्रुवागीतों की परम्परा भरत के पूर्व से लेकर बाण के समय तक भरतोक्त रूप में विद्यमान थी और संभवतः इसलिए भरत ध्रुवा का इतना महत्त्वपूर्ण और व्यावहारिक वर्णन देने में सफल हो सके हैं।
भरत ने नाटकों में गीतों की उचित योजना को बहुत महत्त्व दिया है। वे कहते हैं जैसे कोई भवन उचित प्रकार से निर्मित होने पर भी रंगने या चित्राकारी के बिना शोभा नहीं देता उसी प्रकार नाट्य-प्रयोग भी बिना गीतों के प्रेक्षकों का मनोरंजन नहीं कर सकता। भरत नाट्य में गीत संगीत को महत्ता बार-बार प्रतिपादित करते हैं। किंतु वे यह भी मानते हैं कि सामान्यतः स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण स्त्रिायों के लिये गीत और पुरूषों के लिए पाठ्य उपयुक्त होता है क्योंकि स्त्रिायों की आवाज सहज मधुर और पतली होती है और पुरुषों की बलवान या मोटी होती है।
भरत संगीत को नाट्य की शय्या मानते हैं। वे गान की विशेषता बताते हुए कहते हैं जिसमें सभी स्वर समाविष्ट रहें, वर्णों को वाद्यों की संगति या सहकार से सुंदर बनाया गया हो, तीन स्थानों में सम्बद्ध हो, तीन यति और तीनों मार्गों से युक्त हो, आनन्द या रंजन प्रदान करता हो, जो सम और ललित गुणशाली हो, अलंकारों से युक्त हो, सुख-पूर्वक जिसका प्रयोग किया जा सकता हो और जो मीठापन लिये हो। ये सभी गुण नाट्य में प्रयुक्त गीतों में होने ही चाहिए। इसलिये सर्वप्रथम गीतों पर अध्कि ध्यान देना या प्रयत्न करना चाहिए क्योंकि शय्याभूत गीत ही नाट्य का आधर या विश्राम स्थल होता है। गायन और वाद्यों का ठीक प्रकार से प्रयोग करने पर नाट्य-प्रदर्शन को किसी प्रकार की आशंका या संकट का सामना नहीं करना पड़ता है।
भरत नाटक को यदि एक यज्ञ मानते हैं तो गीत और संगीत को उसका मंत्रोच्चार। नाटक को एक कर्मकांड की तरह व्याख्यायित करने के पीछे उनकी मंशा लोकहितकारी रही है और यों भी प्रारंभ से नाटक लोक-कल्याण के अपने महती लक्ष्य को लेकर चला है। पूर्वरंग का समूचा विधान संगीत या उसके अवयवों से ओतप्रात है। संगीत की अलौकिकता के संदर्भ में कहते हैं कि भरत द्वारा प्रयुक्त पूर्वरंग विधान और उसमें संयोजित गीत-संगीत को देखकर देवता कह उठे-
‘‘‘जब गीत एवं वाद्य की ध्वनि के द्वारा अनुगत शुभावह नान्दी शब्दों का उच्चारण जिस प्रदेश को व्याप्त करेगा तो उससे सभी पापों का नाश हो जायेगा तथा वहां मांगल्य या शुभ दशा ;स्वतः प्राप्त हो जायेगी।’‘
यही कारण है कि संगीत को भरत ने एक सहस्त्र बार पवित्र नदी में स्नान करने या जप-तप कर्म से भी श्रेष्ठ माना है

3 Comments