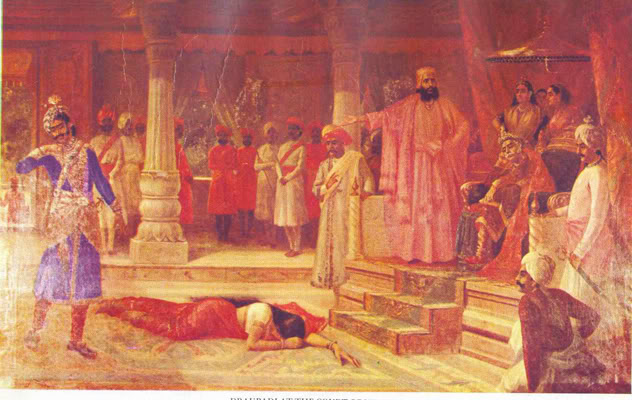
भारतेन्दुयुगीन रंगमंच : संगीत की दृष्टि से
डॉ गुंजन कुमार झा

भारतेन्दुयुगीन रंगमंच : संगीत की दृष्टि से
डॉ गुंजन कुमार झा
नाट्यशास्त्र के चौथे अध्याय में एक कथा उल्लेखित है। जब भरत ने ब्रह्मा के आदेश पर ‘अमृतमंथन’ एवं ‘त्रिपुरदाह’ नामक नाटकों की रचना की तो उसमें संगीत तत्व को अनुपस्थित रखा। इन नाटकों को शिव को दिखाया गया। उन्हें यह पसंद नहीं आया। शिव ने भरत को सलाह दी कि वे इन नाटकों में संगीत और नृत्य का भी प्रयोग करें। इससे अभिनय और नाट्य-प्रदर्शन के स्तर में गहराई और विस्तार आएगा।
भारतेंदु अपने युग के पुरोधा नाटककार थे। तद्युगीन नाटककारों भारतेंदु को ही अपना आदर्श मानकर उनका अनुकरण किया। इनसे पूर्व के नाटक ब्रजभाषा के काव्य नाटक हैं जिसमें संगीत तत्त्व की अधिकता थी। भारतेंदु से जिस भाषा नाटक की शुरुआत हुई वह भी संगीत तत्व से पूर्ण थी। अंतर यह था कि जहाँ भारतेन्दु पूर्व के ब्रजभाषा काव्य नाटकों में ‘संगीत में अभिनय’ का सम्मिलन था वहीं भारतेन्दु युग के नाटकों में ‘अभिनय में संगीत’ का सम्मिलन हुआ।

भारतेंदु युग में जितने भी नाटक लिखे गए प्रायः सभी नाटक गीत-संगीत से पूर्ण थे। भारतेंदु के नाटकों में संगीत तत्त्व पर अलग से बात करेंगे। यहाँ हम उस युग के अन्य नाटककारों पर एक निगाह डालते हैं।
भारतेंदु के प्रसिद्द नाटक के नाम पर प्रतापनारायण मिश्र ने भी ‘भारत दुर्दशा’ नाटक लिखा। यह नाटक संगीतमय नाटक है जिसे लोक शैली में मंचित किया जा सकता है। उन्होंने लावनी के ढंग पर गाने योग्य एक पद्य नाटक लिखा – संगीत शंकुंतालम’। यह खड़ी बोली में है। बद्रीनारायण चौधरी का एक अधूरा नाटक है – ‘वीरांगना रहस्य महानाटक’। यह शृंगार रस के श्लोक, कवित्त, सवैये, गजल, शेर इत्यादि से पूर्ण है। किशोरी लाल गोस्वामी का ‘नाट्य संभव’ , राधाचरण गोस्वामी का ‘अमरसिंह राठौर’ शरत कुमार मुखोपाध्याय का ‘भारतोद्धार’ – ये सभी नाटक गीतों से सजे हुए हैं। शरत कुमार के ‘भारतोद्धार’ नाटक के प्रथम दृश्य में भारतमाता क्रन्दन करते हुए मूर्च्छित आर्यजनों से कहती हैं-
सुन आर्य, सुन बाछा विनय है मोरी
आय गया दिन खोल रे तरबार तोरी।
यह फारसी अति दूरदर्शी मारत है मोय
उठ पुत्र कर मुझको उद्धार
अखंड कीर्ति तव होय।
उधर पूर्व से चले आ रहे ‘रामलीला’ और ‘रासलीला’ संबंधी बहुसंख्य नाटक संगीत प्रधान थे। बलदेव प्रसाद मिश्र कृत ‘प्रभास मिलन’, ब्रजवासी गोप कवि रचित ‘मानचरित्र’ व ‘माधुरी’, विद्याधर त्रिपाठी कृत ‘उद्धवशाठि नाटिका’, राधा चरण गोस्वामी कृत ‘श्रीदामा’, अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ‘रुक्मिणी परिणय’ आदि कुछ उदहारण हैं। ‘रासलीला’ पर आधारित खड्ग बहादुर मल्ल कृत ‘महारास’ महत्वपूर्ण नाटक है। इसका एक गीत देखिये –
कोऊ कहीं लख्यों री गोपाल
व्याकुल फिरति चहुँदिसी उन बिन ये सब ब्रज की बाल
एक घरी नहीं चैन स्याम बिनु हैं सब अति बेहाल
कृपा करौं अब आय मिलौ तुम हे जसुमति के लाल।
इसके अलावा विशेष रूप से संगीत प्रधान नाटकों की भी रचनाएं हुईं जिन्हें ‘संगीत’ कहते हैं। ‘संगीत’ एक तरह से नौटंकी-परंपरा को दृष्टि में रखकर लिखे गये गीति रूपक हैं। आम मत है कि इन्हीं संगीतों से आगे चलकर गीतिनाटकों की साहित्यिक धारा चली। अमानत कृत ‘इन्दरसभा’ व प्रतापनारायण मिश्र कृत ‘संगीत शाकुंतलम’ और गुरू गैबीनाथ कृत ‘संगीत गोपीचंदोपाख्यान’ इसी तरह के नाटक हैं।
नेमीचंद्र जैन का विचार है कि रंगमंच में संगीत जहाँ नाटक को उत्सवधर्मिता प्रदान करता है वहीं गम्भीरतम विचारों को साधारण व सुभाष्य बनाकर उसे तनावपूर्ण होने से बचाता भी है। यह भारतेंदुयुगीन नाटकों पर अक्षरशः लागू होती है। भारतेंदु जिस मूढ़ जनता को जागृत करना चाहते हुए उसके लिए उन्होंने यदि नाटक का ही क्षेत्र विशेष तौर पर चुना उसका एक कारण यह भी था कि नाटक में ‘दिल्लगी’ द्वारा गम्भीर शिक्षा दी जा सकती थी। तद्युगीन नाटकों में संगीत की क्या महत्ता थी इसका संकेत महेश आनंद इस प्रकार देते हैं-
’’प्रस्तुति में संगीत का प्रयोग आवश्यक था। ‘जानकीमंगल’ नाटक के प्रदर्शन के समय मनोरंजन के लिए मध्यांतर में देशी संगीत के कार्यक्रम के चलने का उल्लेख मिलता है। स्वयं भारतेंदु ने इस ओर संकेत किया है: ‘जब जब एक एक विषय समाप्त होगा जवनिका पात करके पात्रगण अन्य विषय दिखलाने को प्रस्तुत होंगे तब-तब पटाक्षेप के साथ ही नेपथ्य में चर्चरिका आवश्यक है क्योंकि बिना उसके अभिनय शुष्क हो जाता है। —जैसे ‘सत्य हरिश्चंद्र’ में प्रथम अंक की समाप्ति में जा चर्चारिका बजै वह भैरवी आदि सबेरे के राग की और तीसरे अंक की समाप्ति पर जो बजै वह रात के राग की होनी चाहिए।’
संगीत प्रधान लोकनाट्य की परंपरा अपने तरीके से जीवंत थी। लोक नाटकों में प्रकाश के अभाव में दृश्यपरिवर्तन की प्रक्रिया से लेकर कच्चे अभिनय में भावों को गहन करने तक का कार्य संगीत द्वारा ही होता है। परदे व प्रकाश के अभाव में दृश्य परिवर्तन का कार्य भी संगीत से ही होता है। नाटकों में ऐसे गायन विद्यमान होते हैं जो एक ही राग और एक ही ताल की बार-बार पुनरावृत्ति करते हैं। इसका इस्तेमाल विविध दृश्यों को जोड़ने, नाट्य व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक ले जाने और साथ ही नाटक की घटना पर विशेष प्रकाश डालने के लिए किया जाता था।
लोक नाट्य-रूपों में रामलीला, रासलीला,नौटंकी,तमाशा, भवाई ,गाथा-गायन, भड़ैंती, स्वांग, ख्याल और मांच तथा साहित्यिक रचनाओं में सट्टक, रासो, रासक, चर्चरी आदि संगीत तत्व की प्रधानता के साथ ही आज तक प्रचालन में हैं।
लोकप्रिय लोकछंदों के गाथाओं की रचना और पाठ समूचे मध्ययुग में अत्यधिक प्रचलित था। मध्ययुगीन कवियों ने इनकी पाठ-प्रतियोगिताओं के अखाड़ों का उल्लेख किया है। ये प्रतियोगिताएं आज भी होती हैं, और उनको वही पुराना नाम, ‘अखाड़ा’ दिया जाता है। लावनी, लहयारी, ख्याल और रसिया के इन ‘अखाड़ों’ ने हिन्दी के इस कोटि के नाटक के उदय और विकास में पूरा योग दिया है। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत में (भारतेंदु युग में) नए साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रभावों से लोकशैली की काव्य-रचनाओं के पाठ करने की यह परंपरा और भी विकसित एवं समृद्ध हुई। छंदों और धुनों में नवीनता लाई गई और एक प्रकार का मिश्रित, लोकप्रिय संगीत विकसित किया गया। इस सामग्री को नाट्य के ढांचे में सजाने के लिए थोड़ी सी नाटकीय कुशलता की अपेक्षा थी। अतः घटनाओं को जोड़ने के लिए एक वाचक ‘रंगा’ की योजना की गई। उचित स्थानों पर नाच-गाने रखे गए और एक दमदार नाट्य रूप विकसित हुआ।
हिन्दी लोकनाटको में ‘ओपेरा’ शैली का ‘नौटंकी रंगमंच’ संगीत प्रधानता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ‘उत्तर प्रदेश का नौटंकी और भगत (आगरा), हरियाणा का सांग, राजस्थान का ख्याल और मध्य प्रदेश का माच आदि कई नाटयरूप एक ही कोटि के ‘आपेरा’-धर्मी नाटक हैं जो संगीत की पुरानी और व्यापक परपरा के अंतर्गत आते हैं।
इन सबसे इतर भारतेंदु के समय ही एक नए तरह का रंगमंच भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका था और जो आने वाले करीब सौ वर्षों तक आम दर्शकों को अपना दिवाने बनाने वाला था – वह था पारसी रंगमंच।

पारसी रंगमंच अपने शबाब पर तो भारतेन्दु के मरणोपरांत ही पहुँचा किंतु अपनी ठोस उपस्थिति उसने भारतेंदु के जीवन काल में ही दर्ज करा दी थी और यह उपस्थिति इतनी संक्रमणकारी थी कि भारतेंदु भी इसके प्रभाव से न बच सके।
पारसी रंगमंच ने जिस नृत्य संगीत प्रधान नाटकों की प्रस्तुति की। भारतेंदु ने उन्हें कुरुचिपूर्ण व अश्लील माना। भारतेन्दु ने पारसी नाटकों का विरोध किया और जनता की रूचि को परष्किृत करने वाले नाटकों की हिमायत की। वहीँ जाने-अनजाने उनहोंने पारसी रंगमंच गुणात्मक प्रभाव भी ग्रहण किया।
पारसी नाटक पूर्णतः नृत्य व गीत-संगीत प्रधान होते थे और इनका प्रस्तुतीकरण तामझामी होने में संगीत का पर्याप्त योग था। इसके संगीत पर जहाँ एक ओर पश्चिमी ‘ओपेरा’ व ‘बैले’ का प्रभाव था वहीं दूसरी ओर संस्कृत और मध्ययुगीन लोकनाट्यों का भी प्रभाव था। वाजिद अली शाह के समक्ष प्रस्तुत ‘इन्दर सभा’ नाटक जिसमें लोक व शास्त्रीय दोनों तरह के संगीत का समन्वयन था ने पारसी नाटकों के गीत संगीत पक्ष को खासा प्रभावित किया।
पारसी नाटकों में विशेष रूप से ख्याल, ध्रुपद, ठुमरी व दादरा आदि का इस्तेमाल किया गया। नाटकों में मौजूद भावुकता और उसका रोमांटिक पक्ष गायन के ही माध्यम से प्रकट होता। ठुमरी और दादरा की गायकी इस हेतु सर्वथा अनुकूल माने गयीं। पारसी रंगमंच पर गाई गई कई ठुमरियाँ और बहुत से दादरे इतने लोकप्रिय हुए कि दर्शक वर्ग बार-बार ‘वन्स मोर, वन्स मोर’ कह-कहकर फरमाइश करते नहीं थकते थे। नाटक का संगीत को सुनने के लिए लोग बार-बार टिकट खरीद कर नाटक देखने आते थे। यह बात हैरतअंगेज है कि पारसी थिएटर की बहुत सारी ठुमरियाँ इतनी अधिक प्रसिद्ध हुई कि इनके ग्रामोफोन रिकॉर्ड ने लोकप्रियता के नए प्रतिमान स्थापित ।इन ग्रामोफोन की बिक्री से संगीत कम्पनियाँ रातों रात मालामाल हो गयीं और उन गायिकाओं और अभिनेताओं को एक बड़ा तबका अपना स्टार मानने लगा था।

पारसी रंगमंच का संगीत भारतीय उपशास्त्रीय , लोक और पाश्चात्य संगीत का मिला-जुला रूप था। यह संगीत जितना लोकप्रिय हुआ उतना स्थायी नहीं। कह सकते हैं कि पारसी रंगमंच में संगीत और नृत्य का इस्तेमाल उस रचनात्मक तरीके से नहीं किया जा सका जो उसे गरिमा प्रदान कर सकती। इसलिए पारसी रंगमंच के साथ-साथ उसमें प्रयुक्त अच्छा सगीत भी असंदर्भित, अप्रासंगिक, बेढंगे प्रयोगों के कारण तद्युगीन बौद्धिकों और संजीदे वर्ग को निराशा ही प्रदान करता था। प्रतिक्रिया देखिये –
“काशी के पारसी नाटकवालों ने नाच घर में जब शकुंतला नाटक खेला और उसमें धीरोदात्त नायक दुष्यंत खेमटेवालियों की तरह कमर पर हाथ रखकर मटक-मटक कर नाचने और ‘पतरी कमर बलखाए’ यह गाने लगा तो डाक्टर धीनो, प्रमदादास मिश्र प्रभृति विद्वान यह कहकर उठ आए कि अब देखा नहीं जाता। ये लोग कालिदास के गले पर छुरी फेर रहे हैं।“
पारसी रंगमंच का दौर हिन्दुस्तानी संगीत के नए युग के सूत्रपात का दौर था। विष्णु नारायण भातखंडे और विष्णु दिगंबर पलुस्कर भारतीय शास्त्रीय संगीत को सामयिक दृष्टि से परिभाषित और सरलीकृत रूप में व्याख्यित कर रहे थे। सदियों से गुरु-शिष्य परंपरा में सीखा-सिखाया जाने वाला शास्त्रीय संगीत अपने इस सरलीकृत और सामान्यीकृत रूप में सांस्थानिक विद्या के लिए तैयार हो रहा था। देशभर में नए और सुगढ़ गायकों की धूम थी किन्तु पारसी रंगमंच से किसी ऐसे संगीतज्ञ के जुड़े होने का पता नहीं चलता है। यहाँ तक कि अलग से संगीत निर्देशक का कोई कॉन्सेप्ट भी उस समय नहीं था और धुन बनाने वालों को या संगीत तैयार करने वालों को हारमोनियम बजाने बजाने के कारण उन्हें ‘पेटीवाला’ ‘पेटी मास्टर’ आदि नामों से संबोधित किया जाता था।
पारसी नाटकों मंचन में समूह गान, एकांकी गान, सवाल-जवाबी गान तथा दो कंठ-गान होता था। ये सभी गान व नृत्य प्रायः विषय से हटकर या विषय में जबर्दस्ती ठूंस कर भरे जाते थे और ठुमरी, ख्याल, ध्रुपद आदि भारी भरकम शास्त्रीय विधाओं के नाम पर भी सस्ते गाने ही पड़ोसे जाते थे। इस कथन को पढ़िए , उर्दू में है किन्तु समझ में आ जाएगा।
“सच यह है कि बम्बई के थेटरों ने (पारसी रंगमंच ने) हिन्दुस्तान को बलिहाज फुनून रक्सो सरफ़द (नाच गाने की कला के लिहाज से) के बेहद नुकसान पहुंचा दिया। सबसे पहले मूसीकी सगीत को तबाह किया और ऐसे वजअ के बेउसूल नगमों को इख्तियार करके बाजारों में फैला दिया, जिनसे जियादःमुहमल (व्यर्थ) कोई चीज नहीं हो सकती।“
औसत विद्वानों का मत है कि इन्हीं कमियों के कारण पारसी थिएटर का संगीत न तो संगीत के लिए महत्त्वपूर्ण बन सकी और न नाटक के लिए। भारतेंदु युग के अन्य नाटकों में भी पारसी रंगमंच के संगीत का प्रभाव था किन्तु उन्हें अलगाते हुए कहा गया है –
“भारतेंदु युग के नाटकों में गाना बजाना तो उन्हीं (पारसी रंगमंच के नाटकों) की ही भाँति होता था, अन्तर इतना ही था कि ये देशोपकारी और धर्मरक्षक होते थे और पारसी नाटकों के गीत-संगीत खालिश मनोरंजन प्रधान होते थे।”
डॉ गुंजन कुमार झा

Leave a Comment